
पिछले पांच सात सालों में राष्ट्रवाद भारत में सबसे केंद्रीय विचार के रूप में उभरा है।अकादमिक विमर्शों से इतर चौक चौराहे और नुक्कड़ की बहसों में भी लोग अपनी समझ के अनुसार राष्ट्रवाद को परिभाषित करते मिल जाएंगे।राष्ट्रवाद भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है।आजादी के लड़ाई में भी राष्ट्रवाद की अहम भूमिका रही है। ऐसे में राष्ट्रवाद और भारतीय राज्य के साथ इसके संबंध को समझना बहुत जरूरी हो जाता है।
आशीष नंदी की किताब "राष्ट्रवाद बनाम देशभक्ति" : रवींद्रनाथ ठाकुर और इयत्ता की राजनीति इस संबंध को परिभाषित करती एक जरूरी किताब है।
यह किताब मुख्यतौर से रवींद्रनाथ के तीन राजनीतिक उपन्यासों का विश्लेषण करता है।इसमें उन राजनीतिक आवेगों और दार्शनिक चेतना का संधान किया गया है जिनके कारण वे राष्ट्रवादी विचारधारा से असहमत होते चले गये।बीच में गांधी का भी यदाकदा आगमन होते रहता है।
रवींद्रनाथ राष्ट्रवाद को पश्चिमी राष्ट्र राज्य प्रणाली की पैदाइश मानते थे। रवींद्रनाथ ने राष्ट्रवाद से सार्वजनिक मोर्चा लिया और अपने प्रतिरोध का आधार भारत की सांस्कृतिक विरासत और नाना प्रकार की जीवन शैलियों को बनाया।
रवींद्रनाथ के लिए भारत की परंपरा ' नस्लों के आपसी समायोजन' के लिए सक्रिय रहती है और ' नस्लों के बीच वास्तविक अंतर को स्वीकार करते हुए एकता का आधार तलाश करती है'। उन्हें यकीन था कि भारत को ' राष्ट्रवाद की वास्तविक अनुभूति कभी नहीं हुई', इसलिए भारत को पश्चिमी सभ्यता से उसके मैदान में प्रतियोगिता करने से कोई फायदा नहीं होगा।
भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रवींद्रनाथ ठाकुर राष्ट्रवाद को भौगोलिक अपदेवता यानी राक्षस करार दे चुके थे।उन्होंने अपना वैकल्पिक विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन इसी राक्षस के प्रभाव से मुक्ति के लिए समर्पित मंदिर के रूप में स्थापित किया था।इस समय तक वे यह घोषित करने की स्थिति में आ चुके थे कि वे तो सभी राष्ट्रों के आधार में निहित आम विचार के ही खिलाफ हैं क्योंकि राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी बुराई बन चुका है।
यहां पढ़िए इस किताब से एक अंश :
कई साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय सिगमंड फ्रायड जैसी अ-राजनीतिक हस्ती ने टिप्पणी की थी कि राज्य की संस्था ने इंसान पर 'दुराचार' करने की पाबंदी लगा दी है, लेकिन यह प्रतिबंध दुराचार खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसे करने की इजारेदारी खुद हासिल करने के लिए लगाया गया है। गांधी और रवींद्रनाथ शायद ही फ्रायड की रचनाओं से वाकिफ रहे हों, पर भारत की राजनीतिक संस्कृति में इस समझ को प्रोत्साहित करने का श्रेय उन्हीं दोनों को जाता है।यह सही है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कठोर हकीकतों और दक्षिणी दुनिया में चली राज्य और राष्ट्र-रचना की शुरुआती प्रक्रिया के दबाव के सामने यह समझ न टिक सकी, पर केवल इसीलिए गांधी और रवींद्रनाथ की असहमति खारिज नहीं की जा सकती।हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम यह कहने की स्थिति में हों कि 18 वीं सदी और 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के यूरोप ने इस बारे में जो कहा था वही अंतिम सत्य नहीं है।हो सकता है कि समय असहमति के इन दो महान पैरोकारों की दृष्टि सही साबित कर दे।





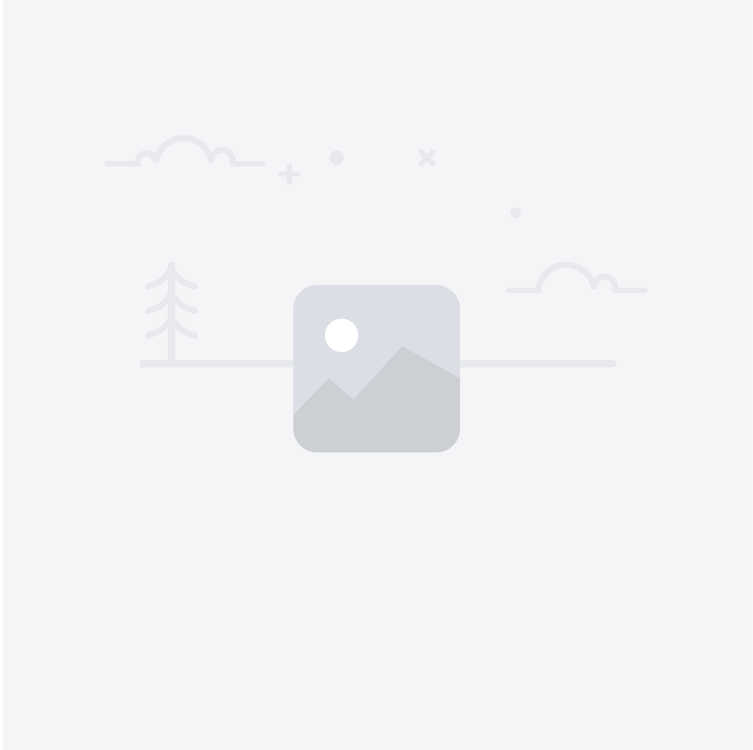

Write a comment ...